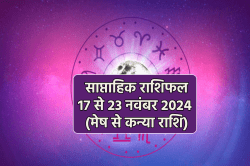Saturday, November 16, 2024
विज्ञान वार्ता : मां ही गुरु, मां ही कृष्ण
सृष्टि जड़ और चेतन के संयोग से ही होती है। प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। ब्रह्म ही पुरुष है। मूल में दोनों एक ही हैं। स्वभाव को ही प्रकृति कहते है।
•Dec 05, 2020 / 08:37 am•
Gulab Kothari
Shri Gulab Kothari articles,Shri Gulab Kothari POV, Shri Gulab Kothari opinion, Shri Gulab Kothari stories,yoga,Gulab Kothari,religion and spirituality,dharma karma,tantra,rajasthan patrika article,gulab kothari article,
– गुलाब कोठारी सृष्टि जड़ और चेतन के संयोग से ही होती है। प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। ब्रह्म ही पुरुष है। मूल में दोनों एक ही हैं। स्वभाव को ही प्रकृति कहते है। चूंकि ब्रह्म और स्थूल सृष्टि के मध्य सात लोक स्थित हैं, अत: प्रत्येक लोक में परिवर्तन आते-आते स्थूल रूप प्रकट होता है। इसी प्रकार लौटते समय भी एक रॉकेट की तरह ब्रह्म प्रत्येक लोक में कुछ-न-कुछ छोड़ता जाता है। छूटने वाले स्वरूप या पदार्थ को मृत्यु कहते हैं। स्थूल शरीर धारण करना जन्म है। स्थूल देह की एक ही भूमिका है-कर्म और फल का भोग। आओ! समझें, गीता क्या कहती हैं-
संबंधित खबरें
‘मुझ से भिन्न दूसरा कोई परम नहीं है। यह सम्पूर्ण जगत् सूत्र (धागे) में मणियों के समान मुझ में गुंथा हुआ है।’ (७/७ गीता) ‘पंचमहाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार ये आठों मेरी अपरा (जड़) प्रकृति के अंग हैं। मेरी दूसरी ‘परा’ प्रकृति जगत् को धारण करती है। यह चेतना है।’ (७/५ गीता)
‘सम्पूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। मैं सम्पूर्ण जगत् का कारण और प्रलय हूं।’ (७/६ गीता) ‘चातुर्वण्र्यम्-चारों वर्ण, तीनों गुण (सत्-रज-तम) तथा कर्म और फल के विभाग, मैं ही रचता हूं। इनका सृष्टा होने पर भी मैं अकर्ता ही हूं।’
ये सारी बातें हमारे जीवन में क्या अर्थ रखती हैं? हमारा शरीर पंचमहाभूतों का तथा पंचकोषों से बना हुआ है। सबसे बाहर स्थूल देह या अन्नमय कोष है। इसके भीतर चारों कोष सूक्ष्म होते हैं। अन्नमय कोष हमारा जड़ भाग है। इसको अन्य शक्ति चलाती है। भीतर प्राणमय-मनोमय-विज्ञानमय कोष हमारा सूक्ष्म शरीर या परा प्रकृति है। केन्द्र में कारण शरीर या आनन्दमय कोष है। सूक्ष्म शरीर अक्षर तथा कारण शरीर के पीछे अव्यय पुरुष हैं। ये पांचों कोष इसकी कलाएं हैं।
शरीर माता-पिता देते हैं। यह अपरा का अंग है। आठों विभाग इस देह में कार्य करते हैं। अन्न से ही पिता का शुक्र बनता है, मन बनता है। शुक्र में पिता एवं उनकी पिछली छ: पीढिय़ों के अंश रहते हैं। शरीर की आकृति पृथ्वी से, प्रकृति चन्द्रमा से तथा अहंकृति सूर्य के प्रतिबिम्बों से उत्पन्न होती है। शरीर मरणधर्मा है। इसका पतन ही मृत्यु है।
अग्नि और सोम के यज्ञ से, जल की आहुति से, पिण्ड का निर्माण होता है। जल से पृथ्वी बनती है। निर्माण के आरंभ में हमारा शरीर भी शुद्ध पिण्ड ही होता है। इसमें जीव नहीं होता। केवल माता के शरीर का अंग बनकर, माता के अन्न से पोषण प्राप्त करता है। अर्थात् शरीर हमारा परिचय मात्र है, हमारा अस्तित्व नहीं है। एक प्रकार से आश्रय है, जिसमें हम जीव रूप में रहते हैं। शरीर की उम्र पूर्ण होने पर हम नया शरीर बदल लेते हैं।
‘जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्यागकर नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को प्राप्त होता है।’ (२/२२ गीता) हम शरीर नहीं हैं, शरीर हमारा रथ है। हम अर्जुन हैं और कृष्ण सारथी हैं। कृष्ण आगे कह जाते हैं कि मैं ही वासुदेव हूं, मैं ही अर्जुन भी हूं। स्वयं अपना सखा। (१०/३७ गीता)
जीवात्मा और ईश्वर दोनों ही सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म हैं। शरीर के सारे कार्य-कलाप भीतर से नियंत्रित होते हैं। किसी चेतन शक्ति के द्वारा। और वह शक्ति (जीवात्मा) शरीर से भिन्न है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि हम किसके लिए जीते हैं-अपने लिए या शरीर के लिए।
जीव तीन माह बाद शरीर में प्रवेश करता है। शास्त्र यह भी कहते हैं कि जीव स्वयं अपना स्थान चुनता है। उसी अनुरूप माता का भी चयन करके गर्भ में अवतरित होता है। उसके बाद गर्भस्थ पिण्ड में हलचल शुरू होती है। तब माता को स्वप्न आने लगते हैं कि यह जीव किस शरीर (योनि) को छोड़कर आया है। उसके संस्कार क्या हैं। कैसे उसे पुन: मानव के रूप में संस्कारित करना है।
जीव अक्षर प्राण के रूप में है। उसके केन्द्र में अव्यय रहता है। वही सबके केन्द्र में भी रहता है। इसके लिए कृष्ण कहते हैं-‘ममैवांशो जीवलोके…’ अक्षर पुरुष की तीन कलाएं-ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र मिलकर ‘हृदय’ (केन्द्र) बनते हैं। बिना केन्द्र के किसी वस्तु का निर्माण नहीं होता। प्रत्येक निर्मित वस्तु अग्नि कहलाती है। सोम अग्नि में आहूत हो जाता है। सोम केन्द्र विहीन (ऋत) होता है। केन्द्र/हृदय में ही परमात्मा रहता है। ‘मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं।’ (१०/२० गीता)
यह आत्मा प्रत्येक जड़-चेतन के केन्द्र में रहता है। इसके लिए कृष्ण स्वयं को अव्यय कहते हैं। सूक्ष्म शरीर जीव की गतिविधियों का मुख्य धरातल होता है। अव्यय पुरुष आलम्बन मात्र होता है। सभी प्राणियों में एकसा रहता है। सूक्ष्म शरीर कारण मात्र रहता है। कार्य सारा स्थूल (क्षर) देह में होता है।
पांचों प्राण और पांचों कर्मेन्द्रियां प्राणमय कोष में रहती हैं। पांचों ज्ञानेन्द्रियां और मन मनोमय कोष के अंग होते हैं। इन ही पांचों ज्ञानेन्द्रियों और बुद्धि से विज्ञानमय कोष बन रहा है। तीनों कोषों से युक्त सूक्ष्म शरीर ही लोकान्तर में भ्रमण करता है। इसका नियंत्रण स्रोत कारण शरीर होता है। इसमें जीव के जन्म के कारण, पूर्व कर्म-फलों का स्वरूप तथा आत्मिक स्वरूप का अज्ञान रहता है। अविद्या के कारण जीव का स्वरूप आवरित रहता है। बन्धन का कारण अविद्या ही होती है। कारणों के अनुरूप ही जीव की आकृति-प्रकृति-अहंकृति बनती है। आकृति और अहंकृति स्थायी भाव रखते हैं। प्रकृति (स्वभाव) के बदलने पर तीनों एक साथ बदल जाते हैं।
जीव जब गर्भ में आता है तब चेतन होता है, पिण्ड जड़ रहता है। जीव का हृदय, पिण्ड के हृदय के साथ जुड़ जाता है। पिण्ड में चेतना प्रवेश कर जाती है। जीव और पिण्ड में अव्यय का स्वरूप एक ही है। वही साक्षी भाव बनता है। जीव अब सीधा माता के सम्पर्क में आ जाता है।
कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने गीता का ज्ञान पहले विवस्वान् को दिया। वह जगत् का पिता होने वाला था। मनु सूर्य से उत्पन्न तत्त्व है। वही ज्ञान, कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। विवस्वान् और अर्जुन दोनों में क्या समानता है? यदि अर्जुन भी कृष्ण ही हैं, तो क्या विवस्वान् भी कृष्ण नहीं है। आज भी वह बारह आदित्यों में से एक हैं। कृष्ण हिमालय भी बता रहे हैं, स्वयं को। अर्थात् जड़-चेतन के हृदय में हैं। वे ही सृष्टि हैं। गीता सम्पूर्ण सृष्टि का, जड़-चेतन सबका ग्रन्थ है। जन्म के कारण, जीवन का स्वरूप और ब्रह्म के साथ जो सम्बन्ध है, वही गीता का ज्ञान है। तब यह ज्ञान सब प्राणियों तक क्यों नहीं पहुंचना चाहिए? और समय के रहते। विवस्वान् को देवासुर-संग्राम (अक्षर-सृष्टि पूर्व), अर्जुन को महाभारत युद्ध से पूर्व यह ज्ञान दिया गया, तब जीव को क्यों नहीं द्वैत में प्रवेश या जीवन-संग्राम में उतरने से पहले दिया जाए! कौन दे?
अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोडऩा कहां सीखा था? माता के गर्भ में। गर्भ में आत्मा के दो धातु होते हैं, जो जीवन का पर्याय बने रहते हैं-ब्रह्म और कर्म। कर्म का सम्पूर्ण क्षेत्र प्रकृति के अधिकार में रहता है। ब्रह्म कोई कर्म नहीं करता। तब प्रकृति रूप में मां को ही प्रथम गुरु बनना होता है। वही गर्भ में सन्तान को संस्कारित करती है। वरना, जो जीव किसी हिंसक प्राणी का शरीर छोड़कर आया, वह मानव शरीर को उसी प्रकार काम में लेगा, जैसे पूर्व शरीर को लेता था।
मां से अपेक्षा है कि उसने ब्रह्म और कर्म के स्वरूप को समझ लिया होगा। मां और सन्तान (गर्भस्थ) का सम्बन्ध सूक्ष्म स्तर पर, आत्म-भाव में रहता है। शरीर भाव में नहीं। जिस प्रकार पिता ब्रह्म का बृंहण (फैलाव) स्वरूप होता है, उसी प्रकार माता भी भर्मण (पालन-पोषण) स्वरूप होती है। गर्भ में ब्रह्म स्वयं कुछ नहीं करता। माता नहीं जानती कि भीतर क्या हो रहा है और क्यों? ब्रह्म का यह बृंहण स्वभाव ही प्रकृति है। मां ही जीव को मानव में रूपान्तरित करती है। जीवन की कला सिखाती है। स्वयं जीव के आत्मा का अंश बनकर अपने जैसा बनाती है। वही जीव है, वही आत्मा है। माता कृष्ण भाव में, आनन्द मग्न होकर, लोरियां गाकर, अपने अर्जुन को तैयार करती है।
कई बार मां स्वयं दीक्षित नहीं होने से इस ज्ञान से अनभिज्ञ होती है। जीव ज्यों का त्यों स्थूल मानव देह धारण कर लेता है। पके घड़े को बदल पाना तो विश्वकर्मा के हाथ में भी नहीं है। माता-पिता मूल रूप में देह के पालक होते हैं। संस्कार पक्ष के अधिकारी, कर्म क्षेत्र के अधिष्ठाता होते हैं। अत: द्वितीय स्थिति में गुरु इस कार्य को हाथ में लेता है। वह संस्कारित करता है, व्यक्ति के आत्मा को। उसका सम्बन्ध सिद्धान्त रूप में ब्रह्म से होना अनिवार्य है। इसके लिए भी गुरु की परीक्षा के प्रावधान हैं।
गुरु व्यक्ति को अपने आत्म-स्वरूप से परिचित कराता है। विद्या से अविद्या के आवरण दूर करता है और अपने समकक्ष बना लेता है। अत: सृष्टि तीन धरातलों पर ही चलती है। ब्रह्म और माया को मैटर और एनर्जी कहा है। दोनों ही स्वत: सृष्टि उत्पन्न नहीं कर सकते। मूल में तो माया भी ब्रह्म की अद्र्धांगिनी है, स्वयं ब्रह्म ही है। वह भी अकर्ता ही है। आत्मा में ब्रह्म और कर्म ही कृष्ण और अर्जुन हैं। गीता आत्मा का ही शास्त्र कहा जाता है। ब्रह्म की साक्षी में जीव जब कर्म क्षेत्र में उतरने लगता है, तब गीता उसे सम्पूर्ण जीवन सृष्टि और जीव के निस्त्रैगुण्य होकर कृष्ण स्वरूप को पा लेने का मार्ग स्पष्ट कर देती है। न मां रहती है, न गुरु, न आत्मा।
Hindi News / Prime / Opinion / विज्ञान वार्ता : मां ही गुरु, मां ही कृष्ण
यह खबरें भी पढ़ें
Jharkhand Election 2024
Maharashtra Election 2024
लेटेस्ट ओपिनियन न्यूज़
Trending Prime News
Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.