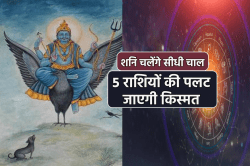दैवो विस्तरश: प्रोक्त आसुरं पार्थ मे श्रृणु ॥’ (गीता16/6) यहां देव और असुर भाव से अभिप्राय मनुष्य के सात्त्विक और तामसिक भावों की अधिकता एवं न्यूनता है। इन्हीं को विद्या तथा अविद्या कहा जाता है।
Saturday, November 16, 2024
विज्ञान वार्ता : भाव शुद्धि से आत्म-साक्षात्कार
कृष्ण कह रहे हैं कि-हे अर्जुन! इस लोक में भूतों (प्राणियों) के स्वभाव दो प्रकार के होते हैं-देवताओं जैसा और असुरों जैसा। जब हृदय में दैवी सम्पद कार्यरूप लेती है तो मनुष्य ही देवता है और जब आसुरी सम्पद का बाहुल्य होता है तब मनुष्य ही असुर है।
•Mar 13, 2021 / 07:29 am•
Gulab Kothari
– गुलाब कोठारी जीवन में जब सारे प्रकाश लुप्त हो जाते हैं तब अंधकार का साम्राज्य छा जाता है। मार्ग में कुछ दिखाई नहीं देता। व्यक्ति तब आत्मप्रकाश के सहारे मार्ग को प्रकाशित रखता है। यह तभी संभव है जब व्यक्ति उस भीतर बैठे ब्रह्म को जान सके। कृष्ण कह रहे हैं कि-हे अर्जुन! इस लोक में भूतों (प्राणियों) के स्वभाव दो प्रकार के होते हैं-देवताओं जैसा और असुरों जैसा। जब हृदय में दैवी सम्पद कार्यरूप लेती है तो मनुष्य ही देवता है और जब आसुरी सम्पद का बाहुल्य होता है तब मनुष्य ही असुर है।
संबंधित खबरें
‘द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च।
दैवो विस्तरश: प्रोक्त आसुरं पार्थ मे श्रृणु ॥’ (गीता16/6) यहां देव और असुर भाव से अभिप्राय मनुष्य के सात्त्विक और तामसिक भावों की अधिकता एवं न्यूनता है। इन्हीं को विद्या तथा अविद्या कहा जाता है।
दैवो विस्तरश: प्रोक्त आसुरं पार्थ मे श्रृणु ॥’ (गीता16/6) यहां देव और असुर भाव से अभिप्राय मनुष्य के सात्त्विक और तामसिक भावों की अधिकता एवं न्यूनता है। इन्हीं को विद्या तथा अविद्या कहा जाता है।
व्यक्ति के भाव ही व्यक्ति को सुर अथवा असुर बनाते हैं। भाव से ही वह राग-द्वेष जैसी वृत्तियों से जुड़ता है। भाव ही तय करते हैं कि उसे आत्मसाधना की ओर बढऩा चाहिए अथवा शक्ति, ऊर्जा और शरीर की ओर। उसी के अनुरूप वह अपनी भावभूमि तैयार करता है। दैनन्दिन जीवन में यही भावभूमि व्यक्ति की चर्या, व्यवहार, कर्म आदि का निर्धारण करती है। सूक्ष्म प्राणों के माध्यम से शरीर में ये भाव परिलक्षित होते रहते हैं। भावना व्यक्ति की सत्ता है, जीवन की दिशा है, यही धर्म है और यही मोक्ष है। वस्तुत:, भाव शब्द तो और भी व्यापक है। इसमें तो सृष्टि, नभ, चित्तवृत्ति, स्वभाव, अवस्था, अभिप्राय, हृदय-आत्मा-मन, संवेग, रस आदि सभी समाहित रहते हैं। भावना से भाव को अभिव्यक्ति मिलती है।
भाव, जीवन की संजीवनी है। स्वस्थ वातावरण और स्वस्थ चिन्तन से अच्छे भाव पैदा होते हैं। अच्छे भाव बनाए रखने का अर्थ है कि पूरा जीवन संयम और साधना में ही गुजरे। सभी प्रकार की दिनचर्या में अनुशासन बना रहे। हर परिस्थिति का सामना कर सकें। विचलन नहीं हो, भय भी नहीं हो और, आनन्द का, सुख का, और निर्मलता का आभास बना रहे।
व्यक्ति की प्रत्येक भावभूमि पहले मन में तैयार होती है। इससे उसके श्वास-प्रश्वास के प्रकम्पन बदलते दिखाई देते हैं। इसके बाद शरीर में हलचल दिखाई देती है। विभिन्न मुद्राएं प्रकट होती हैं, अत: हमारे शास्त्रों में भावभूमि पर ही सबसे अधिक जोर दिया गया है। भाव शुद्ध है, निर्मल और शान्त है, तो आपका व्यक्तित्व भी वैसा ही होगा। सारे धर्म, योग, तप, साधना आदि का पहला लक्ष्य भावभूमि तैयार करना ही है।
मन हमारी भावनाओं का धरातल है। दया, करुणा, राग-द्वेष, सुख-दु:ख, मोह-ईष्र्या, घृणा, हिंसा आदि भावनाएं मन से जुड़ी हैं। व्यक्ति के सात्त्विक, तामसी और राजसी होने का कारण मन है। मन एक ओर तो अति चंचल है, दूसरी ओर इसकी गति विश्व में सबसे तेज भी है। इच्छा मन का बीज रूप है। इच्छा ही जीवन का संचालन मन के माध्यम से करती है। इच्छा को व्यक्ति पैदा नहीं कर सकता। वह नित्य सिद्ध है, सहज ज्ञान से प्रादुर्भूत है। अर्थात् हम जो कुछ हैं और दिखाई पड़ते हैं, वह सब कारण मन के धरातल से निकलता है। मन की यह अभिव्यक्ति बुद्धि और शरीर के माध्यम से होती है। इच्छा का अर्थ है-अभाव, भूख, कुछ पाने की लालसा। तीव्र लालसा ही तृष्णा है। शुद्ध इच्छा ही माया है। जीव को बांधकर रखती है।
भावना में रस होता है, संवेदना होती है, संघर्ष करने की क्षमता बढ़ती है-व्यक्ति तपता है। मन का प्रभाव व्यापक होता है। उसको किसी भाषा की आवश्यकता नहीं है। उसका कार्य भाव प्रधान है, अत: मन के कार्यों में भावों की अभिव्यक्ति जुड़ी रहती है।
भावनाओं के प्रसंग में कृष्णकाल की एक कथा प्रसिद्ध है। रुक्मिणी कृष्ण के पांव दबा रही थी। अचानक उसको लगा कि कृष्ण के पांव में एक छाला हो रहा है। उसने पूछा कि आप तो कभी नंगे पैर चलते ही नहीं, आपके पांव में यह छाला कैसे? कृष्ण सहज रूप से हंस दिए। धीरे से बोले-‘यह तो तुम्हारे कारण हुआ है।’ रुक्मिणी की समझ में कुछ नहीं आया। कृष्ण ने बताया-‘अभी कुछ दिन पहले राधा यहां आई थी। उसके आतिथ्य का भार तुमने उठाया था। एक बार डाहवश तुमने उसको गर्म-गर्म दूध पिला दिया। तुमको नहीं पता कि उसके हृदय में मेरे चरण रहते हैं।’
भावना संस्कारों को परिष्कृत करने का कार्य करती है। जीवन में कहां पहुंचना है, क्या बनना है, आदि बातों को ध्यान में रखकर निर्णय करती है। मन की चंचलता को शान्त रखने में सहायक होती है। व्यक्ति का स्वयं से परिचय कराती है। जीवन का भी यही लक्ष्य है। इसी को योग कहते हैं, स्वयं से स्वयं का योग।
सृष्टि रचना में शरीर सबसे स्थूल भाग है। हमारे अंग-प्रत्यंग, कर्मेन्द्रियां इस स्थूल भाग में समाहित हैं। इसका सूक्ष्म भाग भी है, जिसे ‘प्राण शरीर’ या ‘सूक्ष्म शरीर’ कहते हैं। इसमें हमारे प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोष आते हैं। इसमें हमारी ज्ञानेन्द्रियां, बुद्धि, मन, भेद दृष्टिï, मस्तिष्क आदि हैं। इसके भी भीतर ‘कारण शरीर’ है, जो सदा महत् तत्त्व (चित्त) से जुड़ा रहता है। इसी चित्त के साथ हमारे आत्मा का सम्बन्ध रहता है। व्यवहार में चित्त मूल है। मन, बुद्धि और अहंकार मिलकर चित्त कहलाते हैं। चित्त के कारण ही व्यक्ति स्वयं से आत्मा को अलग स्थापित करता है। इस स्वयं का भासित होना ही अस्मिता है। चूंकि, अहंकार त्रिगुण के प्रभाव से परिवर्तनशील है, अत: सात्त्विक और तामसी भाव में अहंकार को भी अस्मिता कहा गया है। चित्त के साथ राजसी-तामसी चिन्ता और सात्त्विक चिन्तन भी जुड़े रहते हैं।
व्यक्ति का चित्त उसके कार्यों के दौरान भिन्न-भिन्न धरातलों पर आता-जाता रहता है। कभी केवल शारीरिक धरातल पर तो कभी बौद्धिक, मानसिक, आधिदैविक, आधिभौतिक आदि धरातल पर। इन कार्यों के फल भी व्यक्ति को तदनुरूप ही प्राप्त होते हैं। पूर्णमनोयोग से कार्यों में प्रवृत्त हों तभी यज्ञादि कर्मों की पूर्ण सिद्धि होती है।
यज्ञ, मात्र अग्नि में हवन करना ही नहीं है। यह यज्ञ आधिदैविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर रात-दिन हो रहे हैं। इनमें मानव मन के भावों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यज्ञ में जैसे भाव के साथ कामना करें वैसा फल प्राप्त होता है। द्रोणाचार्य से बैर रखने वाले राजा द्रुपद ने पुत्र कामना से यज्ञ किया। किन्तु भाव था कि उनका पुत्र ब्राह्मतेज-क्षात्रतेज से सम्पन्न महाबलशाली द्रोण का वध करे। यज्ञ से उन्हें जुड़वा सन्तान हुई। पुत्र धृष्टद्युम्न और पुत्री कृष्णा (द्रोपदी)। धृष्टद्युम्न ने द्रोण का वध किया। कृष्णा, कौरवों के नाश का कारण बनी। महाभारत के इस एक प्रसंग में भाव की महत्ता को बखूबी समझ सकते हैं।
प्रश्न युधिष्ठिर का था कि मेरे यज्ञ शेष में नेवले का अद्र्धांग स्वर्णिम क्यों नहीं हो सका? कृष्ण का जवाब था कि राजन् यह सत्य है कि आपने राजसूय यज्ञ में प्रभूत मात्रा में दान-पुण्य किया है किन्तु अकालग्रस्त भूख से व्याकुल ब्राह्मण परिवार का दान इसकी तुलना में कहीं अधिक है। जो स्वयं ही भूख से मरणासन्न अवस्था को प्राप्त थे। उन्होंने अपने पास उपलब्ध समस्त सामग्री एक अज्ञात अतिथि की सेवा में अर्पित कर थी। युधिष्ठिर के यज्ञ शेष में नेवले के स्वर्णिम न होने का कारण पाण्डवों के मन में आया अहंकार भाव था। वे अपने दान-पुण्य से स्वयं को ही श्रेष्ठ समझ रहे थे। जबकि यज्ञ, तप और दान आदि सभी कार्यों में भी मन की अहम् भूमिका रहती है। सामथ्र्य के अनुरूप ही व्यक्ति यदि सात्त्विक भावों के साथ यज्ञादि करता है तभी उसका वह सत्कर्म फलित होता है।
यह भी देखें : सूर्य ही महादेव यह भी देखें : विज्ञान वार्ता : सभी एक-दूसरे का अन्न क्रमश:
Hindi News / Prime / Opinion / विज्ञान वार्ता : भाव शुद्धि से आत्म-साक्षात्कार
यह खबरें भी पढ़ें
Jharkhand Election 2024
Maharashtra Election 2024
लेटेस्ट ओपिनियन न्यूज़
Trending Prime News
Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.