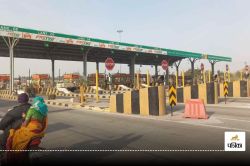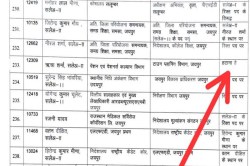ब्रह्म स्थूल शरीर पांच बार में जन्म लेकर प्राप्त करता है। हर स्तर पर पोषण-जन्म-मरण सब माया ही संचालित करती है। मानव शरीर में नारी भूमिका समझकर सभी पांचों स्तरों को समझ सकते हैं। आरंभ के दो स्तर अदृश्य हैं—सूक्ष्म हैं। आगे-आगे के जन्मों/योनियों का संचालन प्रकृति करती है। परा प्रकृति जीव के साथ तथा अपरा का कार्य शरीर से सम्बन्धित अधिक होता है।
ऋग्वेद के अनुसार-
अग्निर्जागार तमृच: कामयन्ते अग्निर्जागार तमु सामानि यन्ति।
अग्निर्जागार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योका:।। प्रलयकाल में सर्वत्र सोम व्याप्त है, अग्नि सुप्त रहता है। समय के साथ और सोमाहुति से ही अग्नि जाग्रत होता है। सोम तुरन्त अग्नि की ओर दौड़ता है। ऋत रूप होने से सोम को आश्रय चाहिए। उसको अग्नि में आहुत होना है—गौण भाव में साथ रहना है। सृष्टि क्रम में सूर्य में आहुत होता है, विद्युत, पृथ्वी, जठराग्नि में (अन्न रूप) आहुत होता है। आगे रेत रूप में पुरुष शरीर से स्त्री शरीर में आहुत होता है। इस आहुति को ग्रहण करके ब्रह्म-विवर्त के विस्तार के लिए ही स्त्री रूप योषा का प्रादुर्भाव हुआ है। स्त्री का आत्मा इस भेद को समझता है। वह ब्रह्म की ही प्रकृति रूपा है। ब्रह्म से भिन्न भी नहीं है।
स्त्री ब्रह्म के बीज को ग्रहण करने पुरुष के पास जाती है। पुरुष का आत्मा उसके सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। उसके रेत में भी उसके सभी अंग-प्रत्यंग का भाग रहता है। स्त्री के प्राण भी पुरुष के हृदय में ही रहते हैं। तब उसके प्राण भी रेत के साथ ही शोणिताग्नि में आहुत होते हैं। मानों रेत के घटक बटोरने के लिए ही वह पुरुष शरीर में बैठी है। दोनों के हृद् प्राण साथ ही रहते हैं। साथ ही सन्तान में जाते हैं।
‘संस्थ्यापन’ (निर्माण एवं पोषण) ही उसका धर्म है। वही ब्रह्म को छिपाकर उसके आवरण का निर्माण करती है। प्रसवकाल तक हर मादा जीव के आत्मा और शरीर का पोषण करती है। मानव नारी को ज्यादा तपस्या करनी पड़ती है क्योंकि मनुष्य योनि कर्मयोनि है। मनुष्य अपने कर्मानुसार अन्य भोग योनियों में जन्म लेता है। प्रसव के बाद भी कई योनियों में माता-पिता शरीर का कुछ काल तक पोषण करते हैं। कहीं स्तनपान से, कहीं चुग्गे से। शिशु शरीर का निर्माण मिट्टी के घड़े जैसा होता है। पूरी उम्र उसकी आकृति नहीं बदलती। शिशु के सम्पूर्ण शरीर में माता के अंश व्याप्त रहते हैं। दोनों का सम्बन्ध सदा बना रहता है। शिशु का मन माता के मन-प्राण-वाक् (शरीर) को पहचानता है। अत: जब भी माता खाना बनाकर खिलाती है, शिशु भोजन को पहचान लेता है। अन्न के चार भाग- दधि-घृत-मधु-अमृत में से केवल अमृत ही मां के आत्मा से प्राप्त होता है। अन्य तीनों की तरह अमृत तत्त्व प्रकृति से सीधा प्राप्त होता है। यह जीव के ईश्वरीय भाव का पोषण है। जब तक मां खाना बनाएगी यह पोषण जारी रहेगा। इसका दूसरा विकल्प भी स्त्रैण भाव ही है। वह पत्नी द्वारा उपलब्ध हो सकता है यदि दोनों का प्रेम एकाकार रूप में है।
पुरुष आत्मा का पोषण पुरुष से होना दुरूह बात है। बुद्धि अमृत से ओत-प्रोत नहीं हो सकती। जगत में पति-पत्नी का ही एकमात्र सम्बन्ध ऐसा है जिसमें कड़वे में भी मिठास रहता है। चन्द्रमा से अन्न-अन्न से मन-मन से मां- मां से मिठास। आत्मिक दृष्टि से पत्नी भी मां ही होती है। वह शरीर सुख के लिए विवाह नहीं करती। उसका उद्देश्य मां बनना होता है। पुरुष उसके लिए निमित्त मात्र है। पुरुष की ही तो मां बनती है। पति ही पुत्र बनता है। दोनों को स्तनपान कराकर प्रकृति के चक्र को सूत्रात्मक आधार प्रदान करती है।
गृहस्थाश्रम के बाद मानसिक पोषण और संन्यास आश्रम में आत्मिक धरातल का साहचर्य प्रदान कर स्वयं अपने आत्मा को पुन: आहुत कर देती है। उसका भीतर का पुरुष जाग्रत-संकल्पित हो पड़ता है। दूसरी ओर पुरुष के भीतर का सौम्य स्वरूप विशेष आकार ग्रहण करने लगता है। वानप्रस्थ में दम्पति रूप में दोनों ही निवृत्ति-भक्ति-सेवाकर्म की ओर बढ़ते हैं। स्त्री की प्रेरणा नेतृत्व करती है। स्त्री अपने सपनों की मूर्ति का निर्माण करने लगती है। तीर्थाटन का नया विषय जीवन से जुड़ जाता है। शनै: शनै: बाहर के जगत से निवृत्त होकर भीतर स्थित होने का, आसक्ति मुक्त होने का, काम-क्रोध-निवारण का मार्ग प्रशस्त किया जाता है।
स्त्री कामना है- सदा मन में रहती है। स्वयं कभी कामना से मुक्त नहीं होती है। किन्तु जिस स्त्री के प्राण पति के हृदय में प्रतिष्ठित रहते हैं, वह पति की सहयात्री बनी रहती है। पति के हृदय का पोषण करती रहती है। अपनी उपासना-तपस्या आदि से भी पति की दीर्घायु की कामना करती रहती है। वह स्वयं भी सर्वेन्द्रिय मन के भीतर महन्मन में प्रविष्ट हो जाती है। पति के अस्वस्थ होने पर पुन: अपने वात्सल्य को प्रकट कर देती है। उसका मातृत्व-अपनापन-संवेदनशीलता का प्रवाह चल पड़ता है। तब पुरुष का अहंकार भी गलता दिखाई पड़ता है। उसकी भी आंखें छलक जाती हैं। यह भी पुरुष मन का पोषण ही तो है। सारे विकार भी परिष्कृत हो जाते हैं।
स्त्री का जन्म भी ब्रह्म-विस्तार तथा पुरुष हृदय के पोषण, पुरुष के प्राकृत-निर्माण एवं परिष्कार के लिए ही हुआ दिखाई पड़ता है। उसका अस्तित्व भी पुरुष के भीतर ही प्रतिष्ठा पाता है। बीज और धरती की तरह दोनों का कार्य अदृश्य रहता है। फल समाज भोगता है। गृहस्थाश्रम में ब्रह्म दोनों के शरीरों से गुजरता हुआ जगत में समा जाता है। दोनों के पास एक ही कार्य बचा रहता है- मोक्षसाक्षी भाव। जिस धर्म के सहारे अर्थ-काम के जीवन से गुजरे, वही धर्म आगे मोक्ष की सीढ़ी बन जाता है।
क्रमश:
gulabkothari@epatrika.com